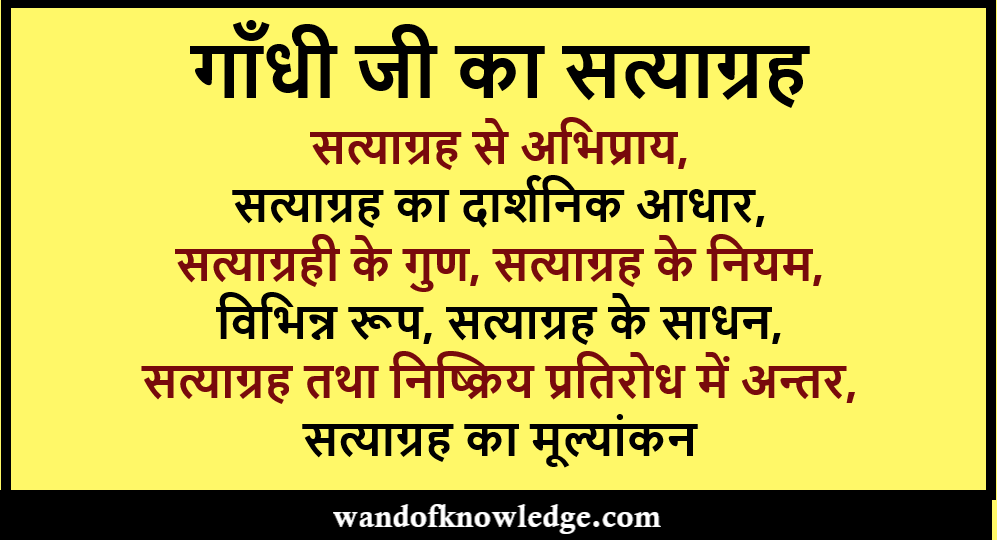
गाँधी जी का सत्याग्रह
गाँधीजी की कार्य-पद्धति : सत्याग्रह
(Gandhian Technique: Satyagraha)
गाँधीजी ने अहिंसा के सिद्धान्त को मूर्त रूप देने के लिए राजनीतिक क्षेत्र में जिस कार्य पद्धति का प्रयोग किया वह सत्याग्रह है। इसके नाम और मौलिक सिद्धान्तों का विकास दक्षिण अफ्रीका में किया गया। वहाँ की गोरी सरकार भारतीयों के प्रति अन्यायपूर्ण कानून पास कर रही थी। इससे वहाँ बसे भारतीयों में तीव्र रोष और असन्तोष था। उन्होंने गाँधीजी के नेतृत्व में इस अन्याय का अहिंसात्मक प्रतिरोध करने का निश्चय किया। उस समय इस आन्दोलन को निष्क्रिय प्रतिरोध’ (Passive Resistance) का नाम दिया गया, किन्तु गाँधीजी को दो कारणों से यह शब्द पसन्द नहीं था। पहला कारण तो इसका अंग्रेजी शब्द होना तथा भारतीयों को इसका पूरा अर्थ समझ में न आना था । दूसरा कारण यह था कि इसमें गाँधीजी द्वारा प्रतिपादित विचारों का पूरा समावेश नहीं होता था। आगे चलकर श्री मदनलाल गाँधी ने ‘सदाग्रह’ शब्द सुझाया। इसका अर्थ है-अच्छे काम में निष्ठा । गाँधीजी को यह शब्द पसन्द आया, किन्तु वे इससे पूर्ण रूप से सन्तुष्ट नहीं हुए। पूरे अर्थ को अभिव्यक्त करने की दृष्टि से उन्होंने इसमें संशोधन करके इसका नाम ‘सत्याग्रह’ रखा।
सत्याग्रह से अभिप्राय
सत्याग्रह का शाब्दिक अर्थ है सत्य के लिए आग्रह करना। इसका आधार है सत्य की अर्थात् सत्य से उत्पन्न होने वाले प्रेम तथा अहिंसा की शक्ति। यह शारीरिक बल अथवा शस्त्रों की भौतिक शक्ति से सर्वथा भिन्न है। यह आत्मा की शक्ति है। सत्याग्रह का संचालन आत्मिक शक्ति के आधार पर किया जाता है। सत्याग्रह के सम्पूर्ण दर्शन का आधारभूत सिद्धान्त यह है कि ‘सत्य की ही जीत होती है।
सत्याग्रह का दार्शनिक आधार
सत्याग्रह का अर्थ है सत्य पर आग्रह करते हुए अत्याचारी का प्रतिरोध करना, उसके सामने सिर को न झुकाना तथा उसकी बात को न मानना । अत्याचारी और अन्यायी को तभी सफलता मिलती है जब लोग भयभीत होकर उसके सामने घुटने टेक दें। किन्तु यदि लोग यह दृढ़ संकल्प कर लें और यह घोषणा कर दें कि ‘तुम चाहे जो करो, हम तुम्हारी आज्ञा का पालन नहीं करेंगे’ तो अत्याचारी शासक उन्हें मरवा सकता है किन्तु उससे अपनी आज्ञा का पालन नहीं करा सकता। जब उसे इस बात का निश्चय हो जाता है कि वह अपने प्रजाजनों को मार डालने पर भी अपनी इच्छा उनसे नहीं मनवा सकता तो वह प्रजा का दमन करना निरर्थक समझता है और इसे छोड़ देता है। इसके अतिरिक्त उसके हृदय पर सत्याग्रहियों द्वारा झेली जाने वाली कठोर यातनाओं और कष्टों का भी प्रभाव पड़ता है। सत्याग्रही द्वारा प्रसन्नतापूर्वक कष्ट झेलने से अत्याचारी में मनुष्यता की प्रसुप्त भावना जागृत हो उठती है। इसके परिणामस्वरूप अन्त में एक ऐसी स्थिति आ जाती है कि अत्याचारी की आँखें खुल जाती हैं, उसे अपने किये अत्याचारों पर पश्चात्ताप होने लगता है। उस समय वह सत्याग्रहियों से समझौता कर लेता है और सत्याग्रह की विजय होती है। यह आत्मबल द्वारा अत्याचारी के हृदय परिवर्तन पर बल देने वाली प्रक्रिया है।
सत्याग्रही के गुण
‘हिन्द साम्राज्य’ में गाँधीजी ने 1908 में सत्याग्रही के आवश्यक गुण सत्यनिष्ठा या ईमानदारी, निर्भयता, ब्रह्मचर्य, निर्धनता और अहिंसा बताये थे। सत्यनिष्ठा का अर्थ है कि सत्याग्रही कभी किसी छल, झूठ या चालाकी का आश्रय नहीं लेता है। निर्भयता सत्याग्रही का एक बड़ा गुण है। उसे सभी बातों में निर्भय होना चाहिए, किसी प्रकार की मोह, ममता न रखकर भूमि, घर, रुपया-पैसा, व्यक्तिगत स्वतन्त्रता तथा जीवन तक का बलिदान करने को तैयार होना चाहिए। ब्रह्मचर्य का अर्थ विषय-वासना के बन्धनों से मुक्त होना है। सत्याग्रही को निर्धनता का व्रत लेने की आवश्यकता है। पैसे का लोभ और सत्याग्रही की साधना दोनों चीजें एक साथ नह हो सकतीं। अहिंसा सत्याग्रह का मूल है, इसका अर्थ है मन, वचन तथा कर्म से अहिंसा अर्थात् शत्रु को न तो मारना-पीटना, न तो कठोर वचन कहना और न मन से उसका बुरा सोचना । हिन्द स्वराज्य में प्रतिपादित उपर्युक्त गुणों में गाँधीजी ने कुछ अन्य गुणों की वृद्धि करके 11 गुणों का पालन और साधना आवश्यक बतायी। ये गुण निम्न हैं-अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, शरीर श्रम, अस्वाद, निर्भयता, सब धर्मों को समान दृष्टि से देखना, स्वदेशी तथा अस्पृश्यता निवारण।
सत्याग्रह के नियम
सत्याग्रह के शस्त्र का प्रयोग बड़ी सावधानी और बुद्धिमत्ता के साथ उस समय करना चाहिए, जब शान्तिपूर्ण रीति से अन्याय का प्रतिकार करने के अन्य साधनों का प्रयोग विफल हो चुका हो । सत्याग्रह शुरू करने से पहले अपनी न्यूनतम माँग निश्चित कर लेनी चाहिए, इस मांग को पूरा करने पर आग्रह करना चाहिए और घोर अत्याचार एवं दमन होने पर भी इस माँग के पूरा होने तक आन्दोलन जारी रखना चाहिए। इसमें अहिंसा का पालन पूर्ण रूप से आवश्यक है। इसका उद्देश्य विरोधी को हराना या नीचा दिखाना नहीं, किन्तु उसका हृदय-परिवर्तन करके उसे अपने अनुकूल बनाना है। यह कार्य सत्याग्रही अपने ऊपर कष्ट झेल कर सकता है।
सत्याग्रही के वैयक्तिक जीवन में गाँधीजी ने प्रधान रूप से निम्नलिखित नियमों के पालन पर बल दिया था-
- सत्याग्रही अपन मन में गुस्से को कोई स्थान नहीं देगा।
- वह विरोधियों के रोष को सहन करेगा।
- ऐसा करते हुए वह बदले की भावना से विरोधियों पर हाथ नहीं उठायेगा। शत्रु द्वारा क्रोधावेश में दी गयी आज्ञा, दण्ड या अन्य किसी प्रकार के भय के सामने अपना सिर नहीं झुकायेगा।
- जिस समय कोई अधिकारी सविनय आज्ञा भंग करने वाले को पकड़ने आयेगा तो वह स्वयं गिरफ्तार हो जायेगा । जब कोई अधिकारी उसकी सम्पत्ति जब्त करने अथवा उसे ले जाने के लिए आयेंगे तो वह उनका प्रतिकार नहीं करेगा।
- यदि सत्याग्रही किसी सम्पत्ति का ट्रस्टी है तो वह इसे सरकार के कब्जे में देने से कार करेगा, भले ही उसके प्राण खतरे में पड़ जायें।
- सविनय कानून भंग करने वाला विरोधियों का भी अपमान नहीं करेगा, ऐसा कोई नारा नहीं लगायेगा जो अहिंसा के विरुद्ध हो।
- इस संघर्ष में यदि कोई किसी अधिकारी का अपमान करता है अथवा उस पर हमला करता है तो सविनय आज्ञा-भंगकारी अपने प्राणों को संकट में डालकर भी उस अधिकारी की रक्षा करेगा।
सत्याग्रह के विभिन्न रूप
गाँधीजी ने भारत के राजनैतिक आन्दोलनों में सत्याग्रह का तीन रूपों में प्रयोग किया-
- असहयोग आन्दोलन (Non-Cooperation)
- सविनय आज्ञा भंग (Civil Disobedience)
- व्यक्तिगत सत्याग्रह (Individual Satyagraha)
इससे पहले दक्षिण अफ्रीका में उनके द्वारा चलाये गये आन्दोलन को ‘निष्क्रिय प्रतिरोध‘ (Passive Resistance) का नाम दिया जाता है। यद्यपि उन्होंने स्वयं इसे ‘सत्याग्रह आन्दोलन’ कहा था तथा निष्क्रिय प्रतिरोध से भिन्न माना था।
- असहयोग आन्दोलन– 1920-21 में गाँधीजी द्वारा चलाये गये आन्दोलन को असहयोग का नाम दिया गया क्योंकि इस समय गाँधीजी ने इस बात पर बल दिया था कि ब्रिटिश सरकार की पराधीनता से मुक्त होने का एकमात्र उपाय भारतीयों द्वारा ब्रिटिश सरकार से सब प्रकार का असयोग करना उनकी नौकरियों को छोड़ना, अदालतों, स्कूलों और कॉलेजों का बहिष्कार करना है। यदि सरकार को शासन कार्य में सहायता देने वाले हजारों व्यक्ति ब्रिटिश सरकार असहयोग कर दें, तो मुट्ठी भर अंग्रेज भारत पर शासन नहीं कर सकते हैं। इससे भारत को अहिंसक रीति से स्वराज्य मिल जायेगा।
- सविनय आज्ञा भंग– गाँधीजी का दूसरा आन्दोलन 1930-31 में सविनय आज्ञा भंग का था । जब ब्रिटिश सरकार ने काँग्रेस के प्रस्ताव के अनुसार भारत को पूर्ण स्वराज्य देना स्वीकार नहीं किया तो गाँधीजी ने ब्रिटिश सरकार के अन्यायपूर्ण कानूनों की अवहेलना करने के लिए सविनय आज्ञा भंग आन्दोलन चलाया। वे ब्रिटिश सरकार द्वारा नमक पर लगाये गये कर को गरीबों के लिए अत्यन्त अन्यायपूर्ण समझते थे। गाँधीजी ने भारतीयों से ब्रिटिश सरकार के ऐसे कानूनों को तोड़ने को कहा और स्वयं गुजरात में समुद्र तट पर स्थित दाण्डी नामक स्थान पर नमक कानून तोड़ने के लिए अहमदाबाद से पैदल प्रस्थान किया।
- व्यक्तिगत सत्याग्रह– 1940-41 में अंग्रेजों द्वारा भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में घसीटने के बाद उन्होंने ब्रिटिश सरकार के विरोध में व्यक्तिगत सत्याग्रह का आन्दोलन शुरू किया, इसमें श्री विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही बनाया गया।
इन तीन अखिल भारतीय सत्याग्रह आन्दोलनों के अतिरिक्त गाँधीजी के नेतृत्व में कई अन्य सत्याग्रह सफलतापूर्वक चलाये गये।
सत्याग्रह के साधन
गाँधीजी ने सामूहिक रूप से बड़े पैमाने पर सत्याग्रह के लिए निम्नलिखित साधनों के प्रयोग का परामर्श दिया–
- असहयोग– किसी देश का शासन उसकी सैनिक शक्ति पर नहीं अपितु जनता के सक्रिय सहयोग पर आधारित होता है। यदि जनता सरकार को यह सहयोग या समर्थन प्रदान न करे तो शासन सर्वथा निराधार होकर शीघ्र समाप्त हो जायेगा। किन्तु असहयोग के समय सत्याग्रही को सर्वथा अहिंसक होना चाहिए।
- सविनय कानून भंग– दूसरा साधन सविनय कानून भंग करने का है। गाँधीजी ने 1930 में सविनय अवज्ञा आन्दोलन चलाया था। इसके द्वारा अन्यायपूर्ण कानूनों की अवहेलना की जाती है।
- उपवास– तीसरा साधन उपवास है। गाँधीजी इसे सबसे अधिक प्रभावक अस्त्र मानते थे। उपवास के दो बड़े प्रयोजन आत्मशुद्धि तथा अन्याय व असत्य के विरुद्ध प्रतिकार है। गाँधीजी उपवास को न केवल आत्मशुद्धि के लिए अपितु दूसरों की शुद्धि के लिए और राजनैतिक समस्याओं को हल करने के लिए भी करते रहे हैं। गाँधीजी ने अपने उपवासों से अस्पृश्यता की और हिन्दू मुस्लिम एकता की समस्याओं का सराहनीय समाधान किया।
- हिजरत या देश–त्याग– यह बहुत पुराना साधन है। गाँधीजी यह समझते थे कि जब किसी देश में शासक के अत्याचार असह्य हो जायँ, तो सत्याग्रही को वह स्थान छोड़कर चला जाना चाहिए। 1928 के करबन्दी आन्दोलन में बारडोली के कृषकों पर जब भीषण अत्याचार किये गये तो गाँधीजी ने उन्हें हिजरत करने की सलाह दी। वहाँ के किसान पड़ोस के बड़ौदा राज्य में चले गये।
- धरना– धरना देकर बैठने का अर्थ है जब तक हमारी बात नहीं मानी जायेगी तब तक हम एक आसन पर स्थिर होकर बैठे रहेंगे। वे शान्तिपूर्ण रीति से धरना देने के पक्षपाती थे।
- हड़ताल– इसका आशय किसी अन्याय का प्रतिकार करने के लिए सारे व्यापार और कारोबार को तथा अन्य सभी दूकानों और कार्यालयों को बन्द रखना है। इसका उद्देश्य सरकार और जनता का ध्यान किसी अन्याय की ओर आकृष्ट करना तथा उसका प्रतिकार करना है। गाँधीजी हड़ताल का प्रयोग विशुद्ध अहिंसक रहते हुए ही करना चाहते थे।
- सामाजिक बहिष्कार– यदि कोई व्यक्ति समाज द्वारा जघन्य या बुरा समझे जाने वाले काम करता है तो उसकी जाति या बिरादरी उसके साथ सभी प्रकार का सामाजिक सम्पर्क रखना बन्द कर देती है, दूसरे शब्दों में इसे हुक्का-पानी बन्द करना कहते हैं। मनुष्य सामाजिक प्राणी है उस पर उसका प्रबल प्रभाव पड़ता है और वह समाज-विरोधी कार्य छोड़ने के लिए बाधित हो जाता है। गाँधीजी ने इस साधन का प्रयोग अहिंसक रूप से किये जाने पर बहुत बल दिया है। अन्याय करने वाले किसी सरकारी अधिकारी का बहिष्कार इस रूप में भी हो सकता है कि उसके घर में काम करने वाले नौकर-चाकर और भंगी काम करना छोड़ दें, उसे दुकानदार खाद्य सामग्री और वस्त्र देने से इन्कार कर दे। डाक्टर उसका इलाज करना बन्द कर दे तो गाँधीजी की दृष्टि में ऐसा करना हिंसापूर्ण दबाव डालना है। किन्तु यदि ऐसे व्यक्ति को अपने सामाजिक समारोहों तथा पर्वो पर निमन्त्रित न किया जाये तो ऐसा बहिष्कार सर्वथा न्यायोचित है।
सत्याग्रह तथा निष्क्रिय प्रतिरोध में अन्तर
गाँधीजी ने दक्षिण अफ्रीका में जब पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग किया तो उसे ‘निष्क्रिय प्रतिरोध’ का नाम दिया गया था। किन्तु सत्याग्रह और निष्क्रिय प्रतिरोध में अन्तर है और इसी कारण से आगे चलकर गाँधीजी ने अपने आन्दोलनों के लिए सत्याग्रह शब्द ही उपयुक्त समझा।
सत्याग्रह और निष्क्रिय प्रतिरोध में निम्न अन्तर है-
- सत्याग्रही अहिंसा के सिद्धान्त को अपना मौलिक तत्व समझता है और किसी भी दशा में इसका परित्याग नहीं करता है किन्तु निष्क्रिय प्रतिरोध में अपनी कमजोरी के कारण नीति के रूप में अहिंसा का पालन किया जाता है न कि मौलिक सिद्धान्त के रूप में।
- निष्क्रिय प्रतिरोध में शत्रु को परेशान करने की भावना पर बल दिया जाता है किन्तु सत्याग्रह में सत्याग्रही स्वयमेव अधिकतम कष्ट झेलता है।
- निष्क्रिय प्रतिरोध निर्बलों का हथियार है और सत्याग्रह वीरों का। सत्याग्रह के लिए जिस हिम्मत की जरूरत होती है वह तोप तथा बन्दूक का बल रखने वाले के पास हो ही नहीं सकती।
- निष्क्रिय प्रतिरोध द्वेषमूलक है, घृणा और अविश्वास पर टिका होता है, इसके विपरीत सत्याग्रह प्रेममूलक है वह शत्रु के प्रति प्रेम और उदारता के भाव रखता है।
- निष्क्रिय प्रतिरोध में रचनात्मक प्रवृत्ति या कार्यों के लिए कोई स्थान नहीं होता है जबकि सत्याग्रही अपने को सेवा की भावना से प्रेरित होकर प्रौढ़ शिक्षा, मद्यपान निषेध, ग्राम सेवा, राष्ट्रभाषा आदि कार्यों में लगा देता है।
सत्याग्रह का मूल्यांकन
युद्ध और क्रान्ति के विकल्प के रूप में राजनीतिक क्षेत्र में सत्याग्रह के साधन का आविष्कार गाँधीजी की एक बहुत बड़ी देन है। सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में उन्होंने सत्याग्रह के शस्त्र का सफलतापूर्वक प्रयोग किया और यह सिद्ध किया कि सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में इसका प्रयोग युद्ध एवं क्रान्ति के समान महत्वपूर्ण है। मार्क्स और लेनिन जिस परिवर्तन को हिंसापूर्ण क्रान्ति से करना चाहते हैं, गाँधीजी ने उसे अहिंसक सत्याग्रह से सम्पन्न किया। फिर भी आलोचक उनकी सत्याग्रह धारणा की निम्न आधारों पर आलोचना करते हैं-
- सत्याग्रह अहिंसा की धारणा के अनुकूल नहीं– आलोचक एक आदर्श के रूप में सत्याग्रह की आलोचना करते हुए कहते हैं कि सत्याग्रह का सिद्धान्त अहिंसा की धारणा के अनुकूल नहीं है। सत्याग्रह का तात्पर्य न केवल हिंसा का निषेध वरन् विरोधी के प्रति भी किसी प्रकार की दुर्भावना का भी अभाव है। अहिंसा का आशय है कि “मनसा, वाचा, कर्मणा किसी भी रूप में हिंसा का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए और विरोधी के मन को भी दुथ्ख नहीं पहुँचाया जाना चाहिए।” आलोचकों के अनुसार सत्याग्रह से उन व्यक्तियों को निश्चित रूप से मानसिक और अनेक बार शारीरिक कष्ट भी पहुँचता है जिनके विरुद्ध इनका व्यवहार किया जाता है। अतः आर्थर मूर इसे ‘मानसिक हिंसा’ (Mental Violence) कहते हैं। आलोचकों द्वारा सत्याग्रह के एक रूप उपवास को आतंकवाद (Terrorism) और राजनीतिक दबाव (Political blackmail) की संज्ञा दी गयी है।
- सत्याग्रह का प्रयोग सभी परिस्थितियों में सम्भव नहीं– आलोचकों के अनुसार प्रत्येक स्थिति में अनेक जगह प्रत्येक प्रकार के लोगों के साथ सत्याग्रह का सफलतापूर्वक प्रयोग नहीं किया जा सकता। स्वतन्त्र समाजों में, जहाँ विवेक, मानवता के प्रति आदर और न्याय विद्यमान हो, सत्याग्रह का भले ही सफलतापूर्वक प्रयोग किया जा सकता हो; परन्तु निरकुंश शासकों और बौद्धिक तथा नैतिक दृष्टि से बहुत अधिक पिछड़े हुए लोगों के विरुद्ध सत्याग्रह की सफलता में निश्चित रूप से सन्देह किया जा सकता है। अनेक बार ऐसा देखा गया है कि शासक वर्ग के द्वारा दमनात्मक बल के आधार पर सत्याग्रह को कुचल दिया गया। विरोधी के अन्तःकरण को जाग्रत करने का कार्य निश्चित रूप से बहुत अधिक कठिन है। डॉ० बन्दुरा के शब्दों में, “इस बात का सामान्यीकरण करना कि सत्याग्रह द्वारा कहीं भी और किसी भी प्रकार के लोग अन्यायी का हृदय परिवर्तन कर सकते हैं, आत्मनाशक है।”
- अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में या आक्रमण के प्रतिरोध में सत्याग्रह का प्रतिरोध सम्भव नहीं– गाँधीजी द्वारा विदेशी आक्रमण की स्थिति में भी सत्याग्रह का सुझाव दिया गया था किन्तु सामान्य अनुभव के आधार पर यही कहा जा सकता है कि ऐसी स्थिति में सत्याग्रह सफल नहीं हो सकता। कोई भी राष्ट्र अहिंसक साधनों पर निर्भर रहकर अपने नागरिकों की स्वतन्त्रता और सुरक्षा खतरे में नहीं डाल सकता । वर्तमान समय में छोटे बड़े देश अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में एक-दूसरे के विरुद्ध जिस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं, उसे देखते हुए तो सत्याग्रह की सफलता बहुत ही अधिक संदिग्ध हो जाती है। आलोचकों के अनुसार हवाई हमले और परमाणु बम के इस युग में आक्रमण के प्रतिरोध हेतु सत्याग्रह की बात हास्यास्पद ही लगती है।
- अहिंसक साधनों से सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन लाना अत्यधिक कठिन– साम्यवादी, अराजकतावादी तथा अन्य क्रान्तिकारी विचाराधारा वाले व्यक्ति गाँधीवादी विचारधारा की आलोचना करते हुए कहते हैं कि सत्याग्रह जैसे अहिंसक साधनों के आधार पर सामाजिक और आर्थिक स्थिति को पूर्णतया बदलने में सफलता प्राप्त नहीं की जा सकती। आलोचकों के अनुसार समाज का धनिक एवं कुलीन वर्ग अपनी स्थिति कभी भी स्वेच्छा से नहीं छोड़ेंगे और सामाजिक तथा आर्थिक जीवन की भीषण विभिज्ञताओं को समाप्त करने के लिए शक्ति का प्रयोग करना आवश्यक होगा।
- सत्याग्रह के नाम के दुरुपयोग की आशंका– सत्याग्रह के विरुद्ध एक आलोचना यह की जा सकती है कि वर्तमान समय में सत्याग्रह के नाम का बहुत अधिक दुरुपयोग किया जा सकता है। विविध पक्षों द्वारा अपने क्षुद्र स्वार्थों की पूर्ति हेतु जो आन्दोलन किये जाते हैं उनके द्वारा उन्हें भी सत्याग्रह कह दिया जाता है जबकि वास्तव में वे सत्याग्रह न होकर दुराग्रह ही होते हैं।
महत्वपूर्ण लिंक
- गाँधीजी के राजनीतिक विचार- राज्य-विहीन समाज, राज्य की विशेषताएं, इत्यादि
- गाँधी जी का राजनीतिक चिंतन- राज्य, शासन, अधिकार, कर्तव्य, राष्ट्रवाद, अन्तर्राष्ट्रीयवाद
- महात्मा गाँधी का जीवन-परिचय
- गांधी जी के धार्मिक और राजनीतिक विचार
- गांधी जी का प्रेरणा स्रोत और सत्य की अवधारणा
- नेहरू का लोकतंत्र पर विचार (Nehru’s View on Democracy)
- नेहरू का एकता और धर्म-निरपेक्षतावाद (Nehru on Unity & Secularism)
- नेहरू का समाजवाद का विचार (Nehru’s idea of Socialism)
- जयप्रकाश नारायण के सामाजिक विचार और जनतन्त्र समाज
- जयप्रकाश नारायण का बिहार आन्दोलन- सेना, जनशक्ति, भूदान आंदोलन
- मानवेन्द्र नाथ राय और मार्क्सवाद (M. N. Roy & Marxism)
- एम एन राय का मौलिक लोकतन्त्र, राष्ट्रवाद और आर्थिक विचार
- मानवेन्द्र नाथ राय का मौलिक मानववाद (Radical Humanism of M. N. Roy)
- अरविन्द घोष के राजनीतिक चिन्तन के आध्यात्मिक आधार
- बाल गंगाधर तिलक का सामाजिक सुधार दर्शन/ सामाजिक विचार
- बाल गंगाधर तिलक के शैक्षिक विचार और कार्य
- बाल गंगाधर तिलक के राजनीतिक विचार- Part I
- स्वामी दयानन्द सरस्वती का राजनीतिक चिन्तन
- दयानन्द का सामाजिक चिन्तन एवं शैक्षिक विचार/ शिक्षा दर्शन
- विवेकानन्द का सामाजिक चिन्तन
- स्वामी विवेकानन्द के राजनीतिक विचार
Disclaimer: wandofknowledge.com केवल शिक्षा और ज्ञान के उद्देश्य से बनाया गया है। किसी भी प्रश्न के लिए, अस्वीकरण से अनुरोध है कि कृपया हमसे संपर्क करें। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। हम नकल को प्रोत्साहन नहीं देते हैं। अगर किसी भी तरह से यह कानून का उल्लंघन करता है या कोई समस्या है, तो कृपया हमें wandofknowledge539@gmail.com पर मेल करें।

